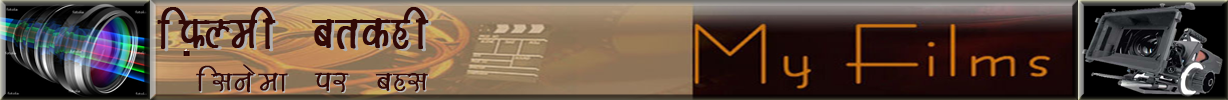Directed & Produced by François Truffaut
Directed & Produced by François TruffautWritten by François Truffaut, Marcel Moussy
Starring: Jean-Pierre Léaud, Claire Maurier, Albert Rémy, Guy Decomble
Music by Jean Constantin. Cinematography: Henri Decaë
Release date(s):
Running time: 99 min. Language: French. Distributed by Cocinor
द ४०० ब्लोज़ फ्रांसुआ त्रूफो की अपनी जीवनी पर आधारित फ़िल्म है। यह फ़िल्म किशोरवय बच्चों के उपर बनी कुछ सबसे अच्छी फ़िल्मों में शुमार की जाती है. इस फ़िल्म में अंटोनी नाम के एक लड़के का बचपन है. उसका बचपन उसके अपने घर में माता पिता की अनदेखी और स्कूल में बहुत ही कठोर किस्म के शिक्षकों के व्यवहार के बीच घुट रहा है. इस घुटन की जानकारी किसी को नहीं है. यह घुटन जब अनजाने में ही अपनी मुक्ति के लिए ज़िंदगी के दूसरे रास्तों पर भटकने लगता है तब क्या - क्या होता है जो उस मासूम अंटोनी के साथ नहीं होना चाहिए था, जिसके लिए वो कत्तई जिम्मेदार नहीं था, इन्हीं कुछ बारीक सवालों और तथ्यों का बहुत ही संवेदनात्मक चित्रण इस फ़िल्म में किया गया है. इस फ़िल्म में आप त्रूफो के बचपन के कुछ बहुत ही व्यक्तिगत पहलुओं का अनुभव करेंगे. फ़िल्म का मुख्य किरदार अंटोनी अपने फ्लैट के पिछवाड़े में बने एक छोटे से कमरे में महान फ्रेंच लेखक बाल्ज़ाक को अपनी भक्ति भावना प्रदर्शित करने के लिए उसके पोस्टर के सामने मोमबत्ती जलाता है और फिर घर में आग लगने जैसी स्थिति पैदा हो जाती है. उसे बाल्ज़ाक की रचनाएं बहुत पसन्द हैं और इसी छोटे से कमरे में अंटोनी बाल्ज़ाक की किताबों में खोया रहता है.
त्रूफो ने इस फ़िल्म में बच्चे की उन सभी हरकतों का जिक्र किया है जिसे हमारे 'सभ्य समाज' में ग़लत कहा जाता है. लेकिन बच्चा यह सब कैसे और क्यों करता है इसका बहुत ही तार्किक sequence इस फ़िल्म में देखा जा सकता है. मसलन, यदि हम उसके स्कूल से शुरुआत करें, तो स्कूल उसके लिए एक ऎसी जगह बन गई है जहाँ परिस्थितिवश उसे अनजाने में ही ज्यादातर शिक्षकों का कोपभाजन बनना पड़ता है, जबकि सामान्यत: उसकी कोई गलती नहीं होती है. शिक्षक उसके साथ एक शैतान बच्चे की तरह व्यवहार करते हैं, उसे बात बात पर सजा दी जाती है और इस तरह का व्यवहार उसके अन्दर एक कुंठित विद्रोही स्वभाव को जन्म देता है. एक 14 साल के बच्चे के शरीर के भीतर एक व्यस्क मानसिकता जन्म लेने लगती है. उसके इन बदलावों को उसके दूसरे कामों में देखा जा सकता है. जैसे वो अपने दोस्त के कहने पर अपने पिता के ऑफिस से टाइपराइटर चुरा लेता है और उसे बेचने की कोशिश करता है लेकिन जब वह इसमें सफल नहीं होता है तो वापस उसे ऑफिस में रखने जाता है जहाँ उसे गार्ड पकड़ लेता है और उसके पिता को बुलाता है. इस सीन में त्रूफो का सिनेमैटिक इंटेलिजेंस दिखता है. जब वह टाइपराइटर रखने जाता है तो उसने एक हैट लगाई होती है जिसे वह पकड़े जाने के बाद उतारने की कोशिश करता है लेकिन गार्ड उसे रोक देता है, वहाँ वह यह साबित करने की कोशिश करता है कि अब यह एक बच्चा नहीं बल्कि एक व्यस्क अपराधी है। पूरी फ़िल्म में अंटोनी के जैकेट का कॉलर हमेशा खड़ा ही रहता है, यह सिर्फ एक सिम्बॉल है उसकी इस सोच का कि वह बड़ों की तरह कुछ भी कर सकता है. बच्चे के माता-पिता उस पर कभी भी बहुत समय नहीं देते हैं जिससे वो उसके अंतरमन को समझ सकें, हमेशा वो उसे उसके द्वारा की जा रही तात्कालिक घटनाओं और दूसरों के द्वारा उसके बारे में की जा रही रिपोर्टिंग (जो कि उसे हमेशा गलत ही समझते हैं) के आधार पर उसका आकलन करते हैं और उसके बारे में अपनी एक मिथ्या राय बना लेते हैं.
फ़िल्म की खासियत यह भी है कि यह एक आम फ्रेंच समाज की कहानी है न कि वहाँ के एलिट वर्ग की. एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार की अपनी समस्यायें हैं और साथ में आधुनिक होने का बोध भी, जहाँ व्यक्तिगत स्वतंत्रता एक बड़ा मूल्य है. इस व्यक्तिगत स्वतंत्रता के नाम पर बच्चे की माँ और उसका सौतेला बाप, दोनों ही उस पर बहुत कम समय देते हैं. हद तो तब हो जाती है जब बच्चे को सजा देने के नाम पर घर से बाहर सामाजिक सेवाओं के भरोसे छोड़ दिया जाता है. यह वो स्थिति है जब बच्चे का मानसिक विकास इतना नहीं हुआ होता है कि वो ये निर्णय ले सके कि उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा, लेकिन वो कुछ न कुछ करता जरूर है. और इस दशा में समाज की नजर में जब उससे कुछ गलत काम हो जाते हैं तो उसके लिए उसे ही दोषी मान लिया जाता है. इस फ़िल्म की कहानी में त्रूफो ने जो सवाल खड़े किए हैं वैसे सवाल हिन्दी साहित्य में मन्नू भन्डारी ने अपने उपन्यास "आपका बंटी" में भी खड़े किए हैं.
यह फ़िल्म पेरिस की भव्यता का वर्णन नहीं करती जहाँ सिर्फ रंगीन fountain हैं, और लुईXVI के स्टाइल के भव्य और बड़े मकान हैं बल्कि इस फ़िल्म में त्रूफो एक आम पेरिसवासी की नज़र से पेरिस को देखते हैं जहाँ वह अपार्टमेंट्स के छोटे छोटे फ्लैट्स के छोटे छोटे कमरों मे सोता है और छ: मंजिले कबूतरखाने से पेरिस की सड़कों पर आने के लिए उपर नीचे दौड़ लगाता है. त्रूफो को फ्रेंच न्यू वेव सिनेमा का मुख्य स्तम्भ माना जाता है. उनकी इस फ़िल्म ने फ्रांस में न्यू वेव सिनेमा की नई इबारत लिखी. यह त्रूफो का अपना तरीका था जहाँ कोई सेट नहीं था बल्कि रोज़मर्रा की ज़िन्दगी में आने वाले आम लोग थे. यह कहानी त्रूफो के अपने बचपन की कहानी भी थी जिसमें उन्होनें ज़िन्दगी की छोटी छोटी हरकतों को अपने कैमरे में बहुत बारीकी से पकड़ा था, जिसमें त्रूफो की अपनी एक अलग झलक
 दिखती है. यदि प्रसिद्ध फ्रेंच फ़िल्म आलोचक आन्द्रे बाज़िन के Auteur Theory की माने तो हर निर्देशक का चीजों को देखने और दिखाने का अपना एक अलग तरीका होता है और यह उसके हर फ़िल्म में झलकता है और एक तरह से वही फ़िल्म का असली लेखक होता है. त्रूफो बाज़िन के सही मायनों में अनुयायी थे.
दिखती है. यदि प्रसिद्ध फ्रेंच फ़िल्म आलोचक आन्द्रे बाज़िन के Auteur Theory की माने तो हर निर्देशक का चीजों को देखने और दिखाने का अपना एक अलग तरीका होता है और यह उसके हर फ़िल्म में झलकता है और एक तरह से वही फ़िल्म का असली लेखक होता है. त्रूफो बाज़िन के सही मायनों में अनुयायी थे.द 400 ब्लोज़ का अंटोनी सुधारगृह में एक सामान्य ज़िन्दगी जी रहा है वह मनोचिकित्सक से बात करता है, यहाँ त्रूफो ने उसका जबर्दस्त आत्मविश्लेशण दिखाया है, वह अपने नए दोस्त के साथ बातें करता है, दूसरे बच्चों के साथ फुटबॉल खेलता है, और फिर जब आप उससे बिलकुल उम्मीद नहीं करते हैं वह वहाँ से भाग जाता है. वह दौड़ता जाता है, दौड़ता जाता है और समन्दर के किनारे पहुंच जाता है, जिसे देखना उसका सपना होता है, वह पानी में दौड़ता है, रुकता है और घूम कर पहली बार सीधे कैमरे में देखता है. त्रूफो ने इस शॉट को फ्रीज़ कर दिया है. इस दृश्य के कई मायने हो सकते हैं लेकिन असली मतलब तो शायद त्रूफो ही जानते हों. यह दृश्य अंटोनी की स्वतंत्रता के साथ साथ यह भी दिखाता है कि पूर्ण स्वतंत्रता जैसी कोई चीज नहीं हो सकती है.
द 400 ब्लोज़ एक masterful निर्देशक की masterpiece फ़िल्म है. त्रूफो इस फ़िल्म से आपको बेज़ुबान कर देते हैं.